मंजरी चतुर्वेदी जीवन को बक्सों और बायनेरिज़ में नहीं रखतीं। सूफी कथक प्रतिपादक जो जल्द ही एक किताब जारी करेंगे कव्वालियाँ भूरे रंग में शानदार ढंग से नृत्य करना पसंद करते हैं। वह एक ऐसे संसार में रहती है जहां भक्ति और रसखान एक साथ विद्यमान हैं। जहां हिंदू और मुस्लिम होली खेलने के लिए एक ही मजार पर इकट्ठा होते हैं। जहां ‘दमा दम मस्त कलंदर’ जैसे हिट गाने लाल शाहबाज कलंदर और झूलेलाल को एक साथ लाते हैं, एक सूफी फकीर, दूसरा एक हिंदू देवता।
एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक पिता और हिंदी साहित्य की विद्वान मां की बेटी, वह लखनऊ में पली-बढ़ीं और लखनऊ से गहराई से प्रभावित थीं। “सूफी, कथक, कव्वालियाँ, तवायफों इसका मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा,” वह कहती हैं, ”आप इसे आत्मसात कर लेते हैं, भले ही यह आपको पाठ्यपुस्तकों में न पढ़ाया गया हो।” यहां तक कि जब उत्तर प्रदेश अपने समन्वित इतिहास को कुचलने के लिए उग्र रूप से प्रयास कर रहा है, तो चतुर्वेदी का कहना है कि संगीतकारों के छोटे-छोटे समूह, जहां वह जाती हैं, अभी भी उस पुरानी दुनिया में रहते हैं जहां भगवान कृष्ण “सहजता से हिंदू धर्म और सूफीवाद की यात्रा करते हैं”।
कव्वाली संगीत से उनका परिचय 1994 में फिल्म निर्देशक मुजफ्फर अली के माध्यम से हुआ, जिन्होंने उनके एक प्रदर्शन में भाग लिया था। शास्त्रीय शैली की सख्त परंपराओं में प्रशिक्षित कथक नर्तक अली उसे लखनऊ के पास सूफी मंदिर देवा शरीफ ले गए। चतुर्वेदी कहते हैं, “मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था। मैंने संगीत सुनना शुरू कर दिया।”

मंजरी चतुर्वेदी का कहना है कि उन्हें सामाजिक मुद्दों को कला के साथ मिलाना पसंद है।
दरवेशों की तरह घूमते हुए
अगले कुछ वर्षों में, चतुर्वेदी पुराने तरीके से खरगोश के बिल में चले गए – पुस्तकालयों में पांडुलिपियों पर ध्यान देना और मध्य एशिया की यात्रा पर, जो मध्ययुगीन युग से सूफीवाद का एक प्रमुख केंद्र था। 1998 में, उन्होंने सूफी कथक को एक नृत्य शैली के रूप में लॉन्च किया। उन्होंने शास्त्रीय नर्तकों द्वारा पसंद किए जाने वाले चमकीले रंगों से परहेज करते हुए काले या सफेद परिधानों में नृत्य किया।
उसका संगीत और नृत्य अब किसी रूपधारी देवता को श्रद्धांजलि नहीं देता था; भक्ति पूरी तरह से भावना के बारे में थी। कथक का चक्रों (स्पिन्स) ने उनकी तकनीकी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया था, लेकिन सूफी कथक में, वह कहती हैं, यह “दरवेशों पर आधारित गतिशील ध्यान” बन गया। प्रेस दयालु थी लेकिन उनके समकालीन और नृत्य गुरु एक शास्त्रीय नर्तक के लोक संगीत पर प्रदर्शन के विचार से नफरत करते थे। एक गुरु ने उनके प्रदर्शन के बीच में ही वाकआउट कर दिया।
जब चतुर्वेदी ने 12 साल पहले कव्वाली पर अपना पहला सेमिनार आयोजित करने की कोशिश की, तो उन्हें शुरुआत में कोई वक्ता नहीं मिला। सेमिनार का सातवां संस्करण, संभवतः आखिरी, इस साल 1 नवंबर को निर्धारित है, और इसमें बातचीत, एक फोटो प्रदर्शनी, उनकी पुस्तक का विमोचन और बहुत कुछ का व्यस्त कार्यक्रम है।
कहानियाँ और स्व-दस्तावेजीकरण
चतुवेर्दी कव्वाली सामान्य ज्ञान का भंडार है। हिंदी सिनेमा ने देश भर के सूफी मंदिरों में गाई जाने वाली कई कव्वालियों की नकल की है, लेकिन ऐसा केवल एक ही उदाहरण है फिल्मी वह मुझसे कहती हैं कि एक दरगाह पर नियमित रूप से कव्वाली गाई जाती है। कैफ़ी आज़मी की ‘मौला सलीम चिश्ती’ से गरम हवा (1974) अक्सर फ़तेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती दरगाह पर गाया जाता है।
उसकी नई किताब, कव्वाली: प्यार में दिलों की पुकारअमीर खुसरो से लेकर दिल्ली के बार में कव्वाली सुनने के अनुभव तक, कला के 700 साल के इतिहास को ट्रैक करता है। काम 14 साल पहले शुरू हुआ जब चतुर्वेदी को एहसास हुआ कि इस सारी संगीत समृद्धि का कोई संग्रह नहीं है। “कव्वाल वे कहती हैं, ”ज्यादातर अनपढ़, हाशिए पर रहने वाले संगीतकार हैं, जिन्हें कभी भी शास्त्रीय गायकों के बराबर नहीं माना जाता।” ”यहां तक कि उनका अपना समुदाय भी उन्हें परंपरा और इतिहास के संरक्षक के रूप में नहीं देखता है।”
चतुर्वेदी ने कव्वाली प्रोजेक्ट शुरू किया, जो अपने अभ्यासकर्ताओं के माध्यम से कव्वाली को संग्रहीत और संरक्षित करने की एक पहल है, जिसमें शक्तिशाली स्व-दस्तावेज़ीकरण पहल ‘आई एम ए कव्वाल’ शामिल है जो अनुमति देता है कव्वाल अपनी कहानियाँ अपने शब्दों में बताने के लिए।
वह कहती हैं, ”मैं आम तौर पर सामाजिक मुद्दों को कला के साथ जोड़ देती हूं, इसलिए प्रायोजक ढूंढने में लंबा समय लगता है।” वह कहती हैं कि उनकी किताब काफी हद तक उनके अपने काम और दो फोटोग्राफर, दिनेश खन्ना और मुस्तफा कुरैशी के प्रयासों के कारण तैयार हुई है। ध्वनि इतिहास संग्राहक अमर नाथ शर्मा को धन्यवाद, उन्हें महिलाओं द्वारा रिकॉर्ड का खजाना मिला कव्वाल.
‘तवायफ’ का खात्मा
चतुर्वेदी के काम ने देश को आकर्षित किया कव्वाल उसे। जल्द ही वह देश के कई समूहों से जुड़ गईं, जो उन्हें सांस्कृतिक पर्यटन पर ले जाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी तरह वजाहत हुसैन बदायूँनी ने लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में प्रदर्शन किया और हैदर बख्श वारसी पुर्तगाल गए। उन्होंने एक फाउंडेशन की स्थापना की जो चिकित्सा सहायता जैसी छोटी-छोटी जरूरतों में मदद करती है और वर्षों बाद, COVID-19 के दौरान, यह प्रणाली काम आई। “मैं सबका हो गया हूं दीदी [elder sister],” वह कहती हैं, ”वे मुझे किसी भी चीज़ के लिए बुलाते हैं, जिसमें वीज़ा फॉर्म भरना भी शामिल है।”
चतुवेर्दी का कहना है कि इस साल का कव्वाली सेमिनार उनका आखिरी सेमिनार होगा। “कव्वाली पर चर्चा और बातचीत के 14 साल हो गए हैं।” वह अब एक और जुनूनी प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं, जो कव्वाली पर उनके काम से पहले ही शुरू हो गया था। यह इस बारे में है कि इतिहास ने इस क्षेत्र की तवायफों को कैसे गलत ढंग से प्रस्तुत किया है। “तवायफों स्वतंत्रता के बाद के युग में सांस्कृतिक संरक्षकों द्वारा जानबूझकर प्रदर्शन कला के इतिहास से हटा दिया गया था, ”वह कहती हैं।
“यह विचार कि तवायफ़ मैं शादी के जरिए मुक्ति का इंतजार कर रही थी और एक ‘अच्छी महिला’ बनने की सीख हमें हिंदी सिनेमा ने दी,” चतुर्वेदी कहती हैं, अपने शोध में उन्हें उनके द्वारा लिखे गए पत्र मिले तवायफों जिन्होंने कहा कि उन्हें शादी करने की कोई इच्छा नहीं है.
एक महिला ने लिखा, “मैं किसी के हरम का हिस्सा नहीं बनना चाहती।” “मैं सिखाता हूं, मैं नृत्य करता हूं। मैं खुश हूं।” चतुवेर्दी यह सुनिश्चित करेंगे कि हम उनकी आवाज़ भी सुनें।
लेखक बेंगलुरु स्थित पत्रकार और इंस्टाग्राम पर इंडिया लव प्रोजेक्ट के सह-संस्थापक हैं।
प्रकाशित – 23 अक्टूबर, 2025 03:22 अपराह्न IST

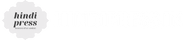



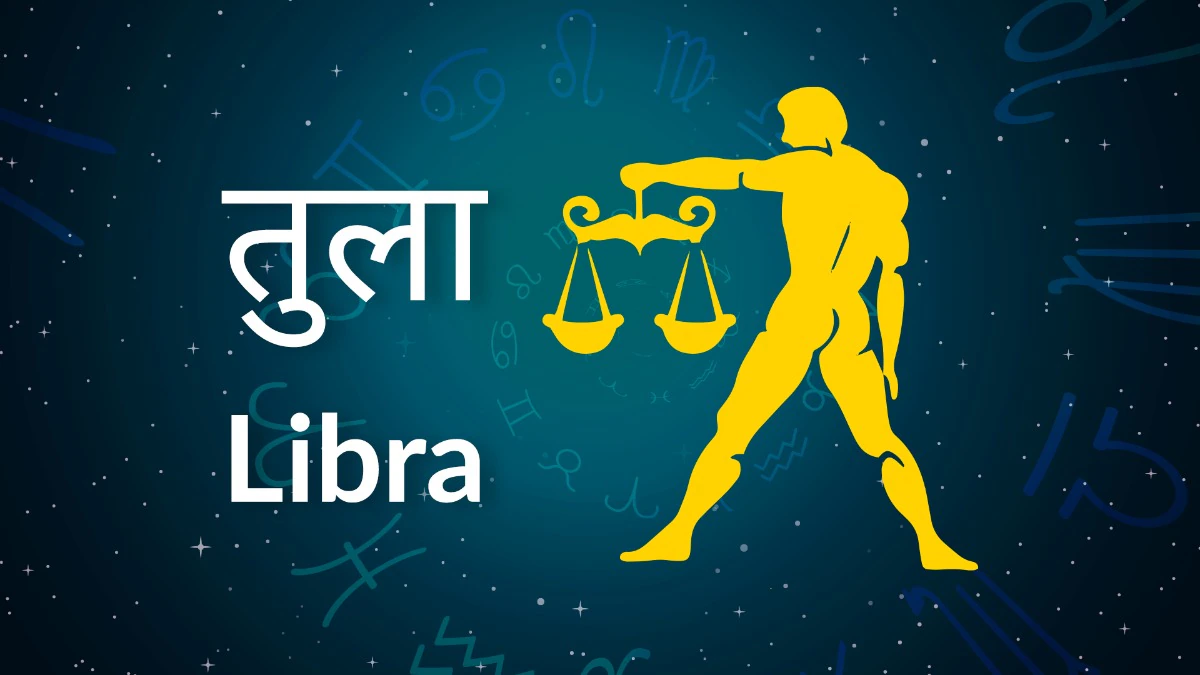

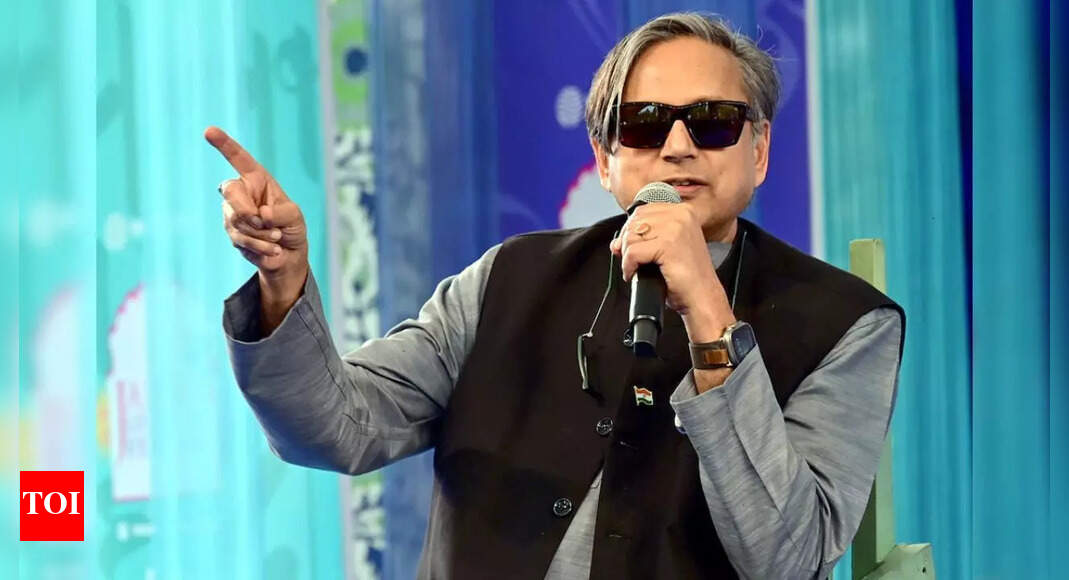




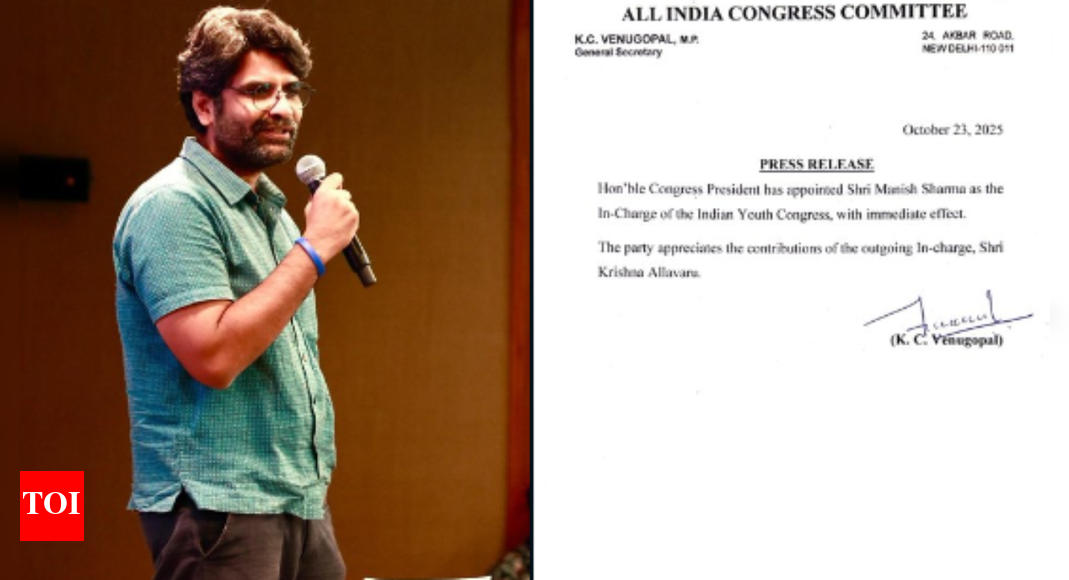



Leave a Reply